संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज और सामाजिक समरसता
Total Views |
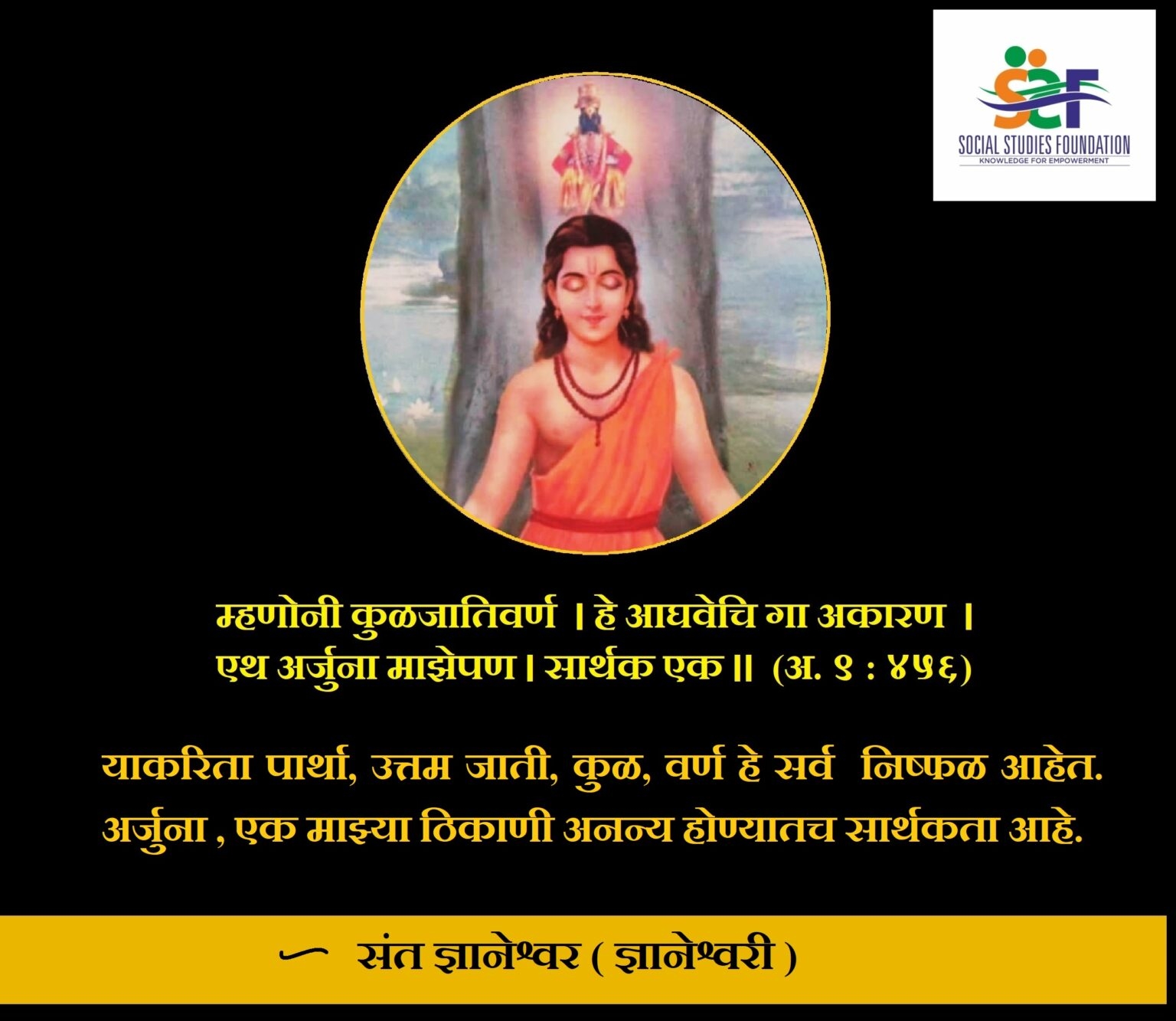
संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज तेरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक महान संत-कवि है। वह भागवत संप्रदाय के प्रवर्तक, योगी और दार्शनिक थे। संत ज्ञानेश्वर जी ने भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी), अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टि, और हरिपाठ में संकलित अभंग ऐसे कई ग्रंथोंकी रचना की है। संत ज्ञानेश्वर ने यह विश्वास पैदा किया कि आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को मराठी जैसी प्रादेशिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसने वैश्विक लोकतंत्र को अपनाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया।
संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म सन 1275 में पुणे के नजदीक आलंदी नाम के गांव में हुआ| उनके पिताजी का नाम विठ्ठलपंत तथा माताजी का नाम रुक्मिणी था| विठ्ठलपंत का परिवार पवित्र और सदाचारी परिवार के रूप में प्रसिद्ध था|
वैराग्य प्राप्त होने के कारन अपने पत्नी की अनुमति लेकर विठ्ठलपंत काशी चले गए थे और वहां संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा के कारन उन्होने फिर एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया| उसके बाद विठ्ठलपंत के कुल चार बच्चे हुए निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई| इसी कारन समाज ने इस परिवार को बहिष्कृत किया था| जब उन्होंने तथाकथित सवर्ण लोगों को अपने परिवार को समाज में फिर से प्रवेश दे कर स्वीकृत करने को कहाँ तब समाज ने इस को न मानते हुए, उनको और उनकी पत्नी को देहांत की सजा सुनाई, जो उन्होंने स्वीकार की| लेकिन नाथ पंथ ने इन गैर जाती परिवार को अपनाया| नाथ पंथ क़े श्री गहिनीनाथ जी ने निवृत्ती को अनुग्रहित किया और वही निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव क़े गुरु हो गए, जो उनके बडे भाई भी थे|
कठोर, हृदयविहीन धर्मशास्त्र का परिचय होने क़े कारन, उन्हें विश्वास था कि सनातन धर्म, जो उन्मूलन और मृत धर्मग्रंथों में डूबा हुआ था, दलित समाज को आत्म-मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकता था। इस बात ने उन्हें भागवत संप्रदाय की स्थापना के लिए प्रेरित किया और कई महिलाओं और शूद्रों के आत्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे शब्दों में, संत ज्ञानेश्वर ने संकेत दिया कि 'ज्ञान की परंपरा सभी मानव जाति की सच्ची विरासत और आधार है'।
संत ज्ञानेश्वर और उनके तीन भाई-बहनों ने कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1290 में, संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवदगीता पर अपनी अलौकिक टिप्पणी पूरी की जो 'ज्ञानेश्वरी' नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर, उनके गुरु निवृत्तिनाथ के कहने पर, संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी स्वयं का स्वतंत्र ग्रंथ, अमृतानुभव या अनुभावमृत की रचना की। संत ज्ञानेश्वर जी को प्यार से वारकरी संप्रदाय सहित सभी भक्तों द्वारा 'माउली' (माता) कहा जाता है| उन्होंने धर्म की आवश्यक बातों को हटाकर धर्म को कर्तव्य का एक अलग अर्थ दिया। साहित्यिक सृजन के साथ, उन्होंने चंद्रभागा तट पर आध्यात्मिक लोकतंत्र के बीज बोने का सफल प्रयास किया। उन्होंने भागवत या वारकरी संप्रदाय की नींव रखने का अभूतपूर्व काम किया। संत नामदेव, संत गोरोबा कुम्हार, संत सावता माली, संत नरहरि सोनार, संत चोखामेला इत्यादि संतोका अनौपचारिक नेतृत्व संत ज्ञानेश्वर ने किया और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इस में से संत नामदेव जी ने पूरे भारत में तीर्थयात्रा की और भागवत धर्म तथा वारकरी संप्रदाय का प्रसार किया।
सन 1296 में, 21 साल की उम्र में, संत ज्ञानदेव जी ने आलंदी में इंद्रायणी नदी के तट पर संजीवनी समाधि की। इस 'ज्ञान के सूर्य' का अस्त होने क़े बाद केवल एक वर्ष के भीतर, उनके भाई-बहन निवृति, सोपान और मुक्ताबाई ने इस दुनिया में अपनी जीवन यात्रा पूरी की।
भागवत धर्म क़े महान उपदेशक संत ज्ञानदेव, एक महान गैर-वैदिक परंपरा के व्यक्ति थे, जिन्हें इस तरह के वैदिक संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी| वह एक विशाल सोच वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म को अलग रखा और बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों के लिए परमार्थ का अधिकार समर्पण किया। यह बहुत स्पष्ट है कि संत ज्ञानदेव और उनके समकालीन संतों ने जातिगत भेदभाव को न मानते हुए अंत्यजादिकों को उपदेश दिया; जो पारंपरिक धर्मशास्त्र द्वारा निषिद्ध था।
ज्ञानेश्वरी में इसी पर अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है की,
म्हणोनि कुळ उत्तम नोहावें । जाती अंत्याहि व्हावें ।
वरि देहाचेनि नांवें । पशूचेंही लाभो ।। (अ. ९ : ४४१)
ते पापयोनीही होतु कां । ते श्रुताधीतही न होतु कां ।
परि मजसीं तुकितां तुका । तुटी नाहीं ।। (अ. ९ : ४४९)
म्हणोनि कुळजातिवर्ण । हे आघवेचि गा अकारण ।
एथ अर्जुना माझेपण । सार्थक एक ।। (अ. ९ : ४५६)
जैसें तंवचि वहाळ वोहळ । जंव न पवती गंगाजळ ।
मग होऊनि ठाकती केवळ । गंगारूप ।। (अ. ९ : ४५८)
कां खैरचंदनकाष्ठें । हे विवंचना तंवचि घटे ।
जंव न घापती एकवटें । अग्नीमाजीं ।। (अ. ९ : ४५९)
तैसें क्षत्री वैश्य स्त्रिया । कां शूद्र अंत्यादि इया ।
जाती तंवचि वेगळालिया । जंव न पवती मातें ।। (अ. ९ : ४६०)
(भावार्थ - जब तक किसी नाले या नदी का पानी गंगा में विलीन नहीं होता है तब तक नाले के पानी को नाला, नदी के पानी को नदी कहा जाता है, लेकिन जब वही पानी एक बार गंगा में विलीन हो जाता है तब उसी नदी या नाले को गंगा ही कहा जाता है। वैसेही खैर की लकड़ी, चन्दन की लकड़ी या किसी अन्य पेड़ की लकड़ी; यह भेद तब तक रहता है; जब तक उन्हें एक साथ आग में नहीं डाला जाता। आग में प्रवेश करते ही सभी लकड़ी एक जैसी ही हो जाती है। इसी तरह, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज और महिलाएं अलग-अलग भेद तब तक मानते है जब तक कि भक्त परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जाति, वंश, वर्ण सभी भेद व्यर्थ है।)
समरस यह शब्द संत ज्ञाननेश्वर का पसंदीदा शब्द है। अनुभव से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही समरस कहा जाता है। संस्कार ही समरसता का मूल है। संस्कार मनुष्य में देवत्व को जगाते हैं। ताकि मनुष्य सामने वाले व्यक्ति में ईश्वर को जान सके। संत ज्ञानेश्वर सहित सभी संतों की प्राथमिकता मनुष्य में देवत्व को जागृत करना था। सद्भाव का रास्ता आध्यात्मिकता से होकर जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी को आस-पास के सामाजिक जीवन में सच्चे धर्म का उज्ज्वल स्वरूप नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने धार्मिक जागरण का काम शुरू किया। वे विरोध की तुलना में समन्वय पर अधिक भरोसा करते हैं। उनकी विचारधारा सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि समन्वित और समग्र है। दलित उत्थान उनके काम का एक प्रमुख हिस्सा था। शूद्रतिशूद्रों को धर्म से जोड़ने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने भगवदगीता का प्राकृत भाषा (मराठी) में अनुवाद किया जिससे उनकी धर्मसाधना अन्तर्मुख हो जाए।
संत ज्ञानेश्वर जी ने निर्माण किया हुआ भागवत संप्रदाय अलग ही था| वारकरी संप्रदाय में कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है| समाज सुधार के लिए आवश्यक कर्मयोग के वह पुरोधा थे| धर्म की तत्कालीन भ्रष्ट और विकृत प्रकृति से उनका परिचय हुआ था| ऐसे समय में धर्म संकल्पना का शुद्धिकरण कर के सर्व समाज को कर्मयोग और भक्ति का मार्ग दिखा के संघटित किया| संत ज्ञानेश्वर जी ने सारे समाज के लिए आत्म-साक्षात्कार का मार्ग खुला करके वर्णाश्रम द्वारा बनाए गए कठोर विनियमन की तीव्रता को कम करने का कार्य करना था। सारे समाज को उन्नति का मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवदगीता का उपयोग किया|
वेदों में, जैसे शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही चारों वर्ण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मूल रूप से वेदों में असमानता का वर्णन नहीं किया गया है। वेदों में और उपनिषदों में जो ज्ञान है, वह तथाकथित शूद्रों के लिए उपलब्ध नहीं था| वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी द्वारा सभी समाज के लिए संत ज्ञाननेश्वर ने मुक्त किया| यह कार्य तत्कालीन धर्म कल्पना के विरोधी था| ज्ञान किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि सभी के लिए वह मुक्त होना चाहिए ऐसी उनकी धारणा थी| परमार्थ के क्षेत्र में वर्ण और जाती-व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है इसी धारणा को लेकर उन्होंने जाती-व्यवस्था नष्ट करने का प्रयास किया|
संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति मार्ग की स्थापना करके महाराष्ट्र के जीवन में एक नए युग की शुरुआत की; केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मध्यकालीन भारतीय धर्म को एक नई राह दिखाई। उन्होंने ब्राह्मणवाद के ढांचे को तोड़ दिया। संत ज्ञानेश्वर के बाद सभी जातियों में संत पैदा हुए इसका विशेष रूप से महत्व है। यह भारतीय संस्कृति में एक चमत्कार है। आत्मोन्नति और जाती व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, यह बात भागवत संप्रदाय ने सिद्ध करके दिखाई| कई शताब्दियों तक हीन समझे जाने वाले लोगों के मन में एक नए आत्मविश्वास को जन्म दिया और उसके व्यक्तित्व की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही संत ज्ञानेश्वर ने ब्रह्मविद्या के भंडार को सभी के लिए खोला, तथाकथित दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने विश्वास के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया।
संत साहित्य का गहरा अध्ययन करने वाले विद्वान् श्री गं. बा. सरदार कहते है “संतो ने जो आंदोलन खड़ा किया उस में धर्म सुधार और जनजागृति की भावना जरूर थी लेकिन समाजिक क्रांति की ललकार नहीं थी| वारकरी संप्रदाय ने महिला-शूद्रों की जड़ता को मिटा दिया और उनके जीवन में कर्म करने की निष्ठा पैदा की। सामाजिक विषमता के कारन बहुजन समाज के मन में जो एक हीनता का भाव पैदा हुआ था, वह मिटाने के लिए और उनकी प्रगति के लिए नए मूल्यों का परिचय करवाया| संत आंदोलन एक प्रतिक्रियावादी शक्ति नहीं थी, जो लोगों को सामाजिक संघर्ष से दूर रखती थी, बल्कि धार्मिक जीवन के दायरे में उनके अधिकारों के लिए लड़ने की एक सुधारवादी प्रवृत्ति थी।“
संत ज्ञानेश्वर के साहित्य में प्रतिबिंबित नैतिकता की उनकी भावना और दलितों के लिए उनकी करुणा सभी उनके कश्मीरी शैववाद दर्शन और भक्ति में निहित हैं। यादव काल का समाज, यादव-पूर्व धार्मिक व्यवस्था के दुष्प्रभाव से पीड़ित था। यह कहते हुए कि दुनिया भगवान की चेतना का विलास है, संत ज्ञानेश्वर ने समाज के विभिन्न स्तरों और तत्वों में एकता का संबंध स्थापित किया। वे परंपरा-स्वीकृति और परंपरा-त्याग के दो चरम को समेटने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता तैयार किया है।
उन्होंने सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जाति व्यवस्था को आध्यात्मिक संदर्भ में खारिज कर दिया है। समतावादी और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में जाति के लिए कोई जगह नहीं है, यह विचार संत ज्ञानेश्वर ने प्रस्थापित किया। वारकारी संप्रदाय के भविष्य पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। संत ज्ञानेश्वर जी के समय में सभी स्तरों के संतों का मेला एक ही झंडे के नीचे इकठ्ठा होता है, यह संत ज्ञानेश्वर की समन्वय की भूमिका का परिणाम है। इस अर्थ में भी, उन्होंने महाराष्ट्र में आध्यात्मिक समानता के आधार पर नए सामाजिक ढांचे की नींव रखी।
यादव-पूर्व और यादव-युग में शैव-वैष्णव विवाद समाज में भ्रम पैदा कर रहा था। इस समय, संत ज्ञानेश्वर ने केवल समाज के कल्याण के लिए शिव और विष्णु एक ही हैं इस विचार को व्यक्त करने का साहस किया। वर्णवाद, जातिवाद, संप्रदायों और साधनों का एकांतिकता, समाज में विभाजन और इसके परिणामस्वरूप असमानता आदि यादव समाज के जीवन की पीड़ाएं थीं। इन पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने समन्वय की योजना की| इस योजना का दीर्घकालीन परिणाम महाराष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास पर हुआ है| संत ज्ञानेश्वर की इस कार्य को महाराष्ट्र कैसे भूल सकता है?
यादव कल में समाज में दरारें पैदा हुई थी| जब तक सभी समाज एक नहीं होता तब तक समाज की भौतिक और पारमार्थिक प्रगति नहीं हो सकती ऐसी संत ज्ञानेश्वर की श्रद्धा थी| हर और हरी में कोई भेद नहीं है यह विचार दे कर, संत ज्ञानेश्वर ने लोगों के मन में एकता की भावना पैदा की। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग का समन्वय करके एकता का संदेश दिया। यह उनके सामाजिक ज्ञान का पहला संकेत था।
संत ज्ञानेश्वर के समय में, समाज के महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाले महिलाओं और शूद्रों को मुक्ति का अधिकार नहीं मिला था। संत ज्ञानेश्वर ने इसका विरोध किया और सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। इसी के परिणाम स्वरुप विघटित समाज वारकरी संप्रदाय के रूप में संघटित हो गया| संत ज्ञानेश्वर के चारों ओर एकत्रित विभिन्न जातियों और जनजातियों के संतों का प्रभाव उनके आध्यात्मिक समतावादी सोच का परिणाम था।
संदर्भ
1) ज्ञानदेव आणि ज्ञानदेवी - संपादक रा. चिं. ढेरे, श्रीविद्या प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती 1991
2) आठव: ज्ञानदेवांचा, ज्ञानदेवीचा - डॉ. यू. म. पठाण, मधुराज पब्लिकेशन्स, प्रथम आवृत्ती 1992
3) सार्थ ज्ञानेश्वरी - संपादक शं. वा. दांडेकर, प्रसाद प्रकाशन, तिसरी आवृत्ती 1962
4) ज्ञानेश्वरी सांकेतिक शब्द दर्शन - पांडुरंग दत्तात्रय देशपांडे, उत्कर्ष प्रकाशन
धनंजय सप्रे
99234933344